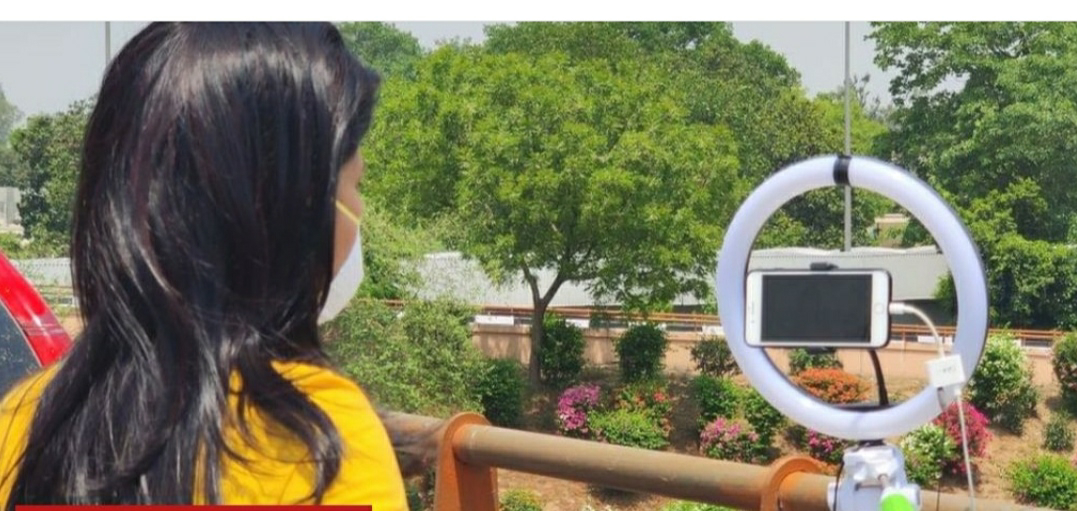आज भारत-चीन सीमा पर तनाव के समय कुछ लोग अपना पुराना टीवी सड़कों पर पटक विरोध जता रहे हैं। चीनी सामान का बॉयकॉट करने के लिए जो पहली शर्त है, वह यह है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन-कौन से सामान में चीन के पैसे लगे हैं। तो इसे जानने के लिए आपको अच्छा-खासा इकोनोमिक एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत पड़ेगी। किस भारतीय प्रॉडक्ट में चीन की एसेसरीज लगी है और किस चीनी प्रॉडक्ट की फैक्ट्री भारत में लगी है, जहां भारतीयों का पैसा लगा है और उन्हें काम मिल रहा है, यह पूरी तरह से पता लगाना एक जटिल काम है। आम आदमी के लिए ये बेहद मुश्किल है।
- पेटीएम, पेटीएम मॉल, बिग बास्केट, ड्रीम 11, स्नैपडील,फ्लिपकार्ट, ओला, मेक माई ट्रिप, स्विगी,
जोमेटो जैसी स्टार्टअप कंपनियों में चीन की अलीबाबा और टेंसट होल्डिंग कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी है।
- भारत में पिछले पांच साल में स्टार्टअप कंपनियों में चीन ने 4 बिलियन डॉलर यानी 30,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कुल इन्वेस्टमेंट का 2/3 भाग है।
- ओप्पो, वीवो, शाओमी जैसे मोबाइल, जिनका भारत के 66% स्मार्टफोन बाजार पर कब्ज़ा है, वे चीनी कंपनियां हैं।
- देश भर की सभी पॉवर कंपनियां अपने ज्यादातर इक्विपमेंट चीन के बनाए खरीदती हैं। TBEA जो भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एक्सपोर्टर कंपनी है, वह एक चीन समर्थित कंपनी है, जिसकी फैक्टरी गुजरात में लगी है।
- देश में बनने वाली दवा के 66% इनग्रेडिएंट्स चीन से आते हैं।
- भारत में उत्पादित समान का चीन तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर देश है। 2014 के बाद भारत का चीन से इम्पोर्ट 55% और एक्सपोर्ट 22% बढ़ा है। भारत चीन के बीच लगभग 7.2 लाख करोड़ का व्यापार होता है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ भारत एक्सपोर्ट और 5.8 लाख करोड़ का इम्पोर्ट करता है।
- इंडियन इलेक्ट्रिक ऑटो सेक्टर तो पूरी तौर पर चाइनीज कंपनी के चंगुल में आता जा रहा है। गिले, चेरि, ग्रेट वॉल मोटर्स, चंगान और बीकी फोटॉन जैसी चीनी कंपनियां अगले 3 साल में 5 बिलियन डॉलर यानी 35 हजार करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट करने जा रहीं। इनमें कई की फैक्ट्रियां मुंबई और गुजरात में लग रही हैं।
- अडानी समूह ने 2017 में चीन की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक ईस्ट होप ग्रुप के साथ गुजरात में सौर ऊर्जा उपकरण के उत्पादन के लिए $ 300 मिलियन से अधिक का निवेश करने का समझौता किया था। रेन्युवेबल एनर्जी में चीन की लेनी, लोंगी, सीईटीसी जैसी कंपनियां भारत में 3.2 बिलियन डॉलर यानी 25 हजार करोड़ से अधिक इन्वेस्ट करने वाली हैं।
- आनंद कृष्णन के एक लेख के अनुसार 2014 में भारत चीन का इन्वेस्टमेंट 1.6 बिलियन था, जो मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद केवल 3 वर्ष यानी 2018 में पांच गुना बढ़कर करीब 8 बिलियन डॉलर हो गया।
- 2019 अक्टूबर में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) में चीनी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (CASME) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसमें उच्च तकनीक क्षेत्रों में चीन 10,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। यह प्रक्रिया उस वक़्त शुरू हुई जब प्रधानमंत्री गुजरात में शी जिनपिंग को झूला झूलाने के लिए लाए थे।
- हाल ही में दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए 1100 करोड़ का ठेका चीनी कम्पनी SETC को मिला है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के साथ चीनी वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स (जीडब्ल्यूएम) का 7600 करोड़ रुपये के निवेश का समझौता हुआ है।
तो ये बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी सरकारी कंपनियां, जो पहले से ही खस्ता हालात में हैं, वहां चीनी समान के उपयोग पर प्रतिबंध केवल फैंटा मंडली और चाटुकार मीडिया को चटखारे लगाने के लिए लगाया गया है। यदि सरकार सच में चीनी उत्पाद का बॉयकॉट करने लगे तो सबसे ज्यादा नुकसान उसके गुजराती परम मित्रों को ही होने वाला है, जो उसके चुनाव खर्चे उठाते हैं।
यदि सच में भारत बॉयकॉट चीन चाहता है तो उसके लिए लंबी, कुशल और दूरदृष्टिसम्पन्न रणनीति की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो सरकार चीनी कंपनियों के लगातार बेताहाशा इन्वेस्टमेंट के बाद भी देश की चलती फिरती अर्थव्यवस्था को 8 से 3.5% जीडीपी पर ले आए, उससे आप बॉयकॉट चीन के मसले पर कितनी आशा रख सकते हैं?
By
डॉ घपेश पुंडलिक राव ढवळे नागपुर
ghapesh84@gmail.com
M. 8600044560