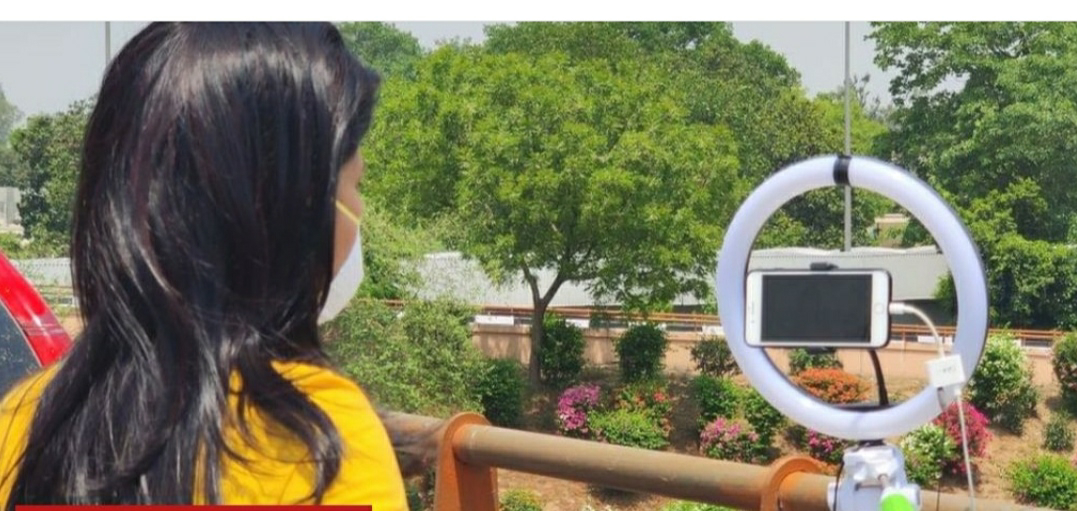*मेडीकल* प्रवेशासाठी लागणारी कागदपत्रे
-----------------------------------------------
1) *नीट* आँनलाईन *फाँर्म* प्रिंट
2) *नीटप्रवेश* पत्र
3) *नीट मार्क* लिस्ट
4)10 वी चा मार्क मेमो
5)10 वी सनद
6) 12वी मार्क मेमो
7) नँशनँलीटी सर्टीफिकेट
8 रहिवाशी प्रमाणपत्र
9)12 वी टी सी
10) मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस
11) आधार कार्ड
12) उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा फाँर्म नं 16 वडिलांचा
13) मुलाचे राष्ट्रीय बँकेतील खाते
14) मुलाचे तसेच आई व वडिलांचे दोघांचे पँन कार्ड
मागासवर्गीयांसाठीवरील सर्व व खालील प्रमाणपत्रे
1) जातीचे प्रमाणपत्र
2) जात वैधता प्रमाणपत्र
3) नाँन क्रिमीलीयर प्रमाणपत्र
( मागील काढलेले असेल तर 31 मार्च2021 पर्यत लागू)
----------------------------------------------------
कृपया वरील कागदपत्रे अपुर्ण असतील तर त्वरीत पुर्ण करून घ्यावे.
----------------------------------------------------
👉🏿 *इंजिनीअरिंग* प्रवेशासाठी लागणारी कागदपत्रे👈🏿
----------------------------------------------------
1) *MHT-CET* आँनलाईन *फाँर्म* प्रिंट
2) MHT-CET* पत्र
3) MHT-CET* मार्क लिस्ट
4)10 वी चा मार्क मेमो
5)10 वी सनद
6) 12वी मार्क मेमो
7) नँशनँलीटी सर्टीफिकेट
8 ) रहिवाशी प्रमाणपत्र
9)12 वी टी सी
10) आधार कार्ड
11) उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा फाँर्म नं 16 वडिलांचा
12) राष्ट्रीय बँकेतील खाते 13) फोटो.
----------------------------------------------------
*मागासवर्गीयांसाठीवरील सर्व व खालील प्रमाणपत्रे*
----------------------------------------------------
1) जातीचे प्रमाणपत्र
2) जात वैधता प्रमाणपत्र
3) नाँन क्रिमीलीयर प्रमाणपत्र
( मागील काढलेले असेल तर 31 मार्च2021 पर्यत लागू)
कृपया वरील कागदपत्रे अपुर्ण असतील तर त्वरीत पुर्ण करून घ्यावे
----------------------------------------------------
*वैद्यकीय क्षेत्र*
------------------------
*शिक्षण - एमबीबीएस*
कालावधी - पाच वर्षे सहा महिने
पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र आणि NEETप्रवेश परीक्षा
संधी कोठे? - स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालयात नोकरी
----------------------------------------------------
पुढील उच्च शिक्षण - एमडी, एमएस व इतर पदविका
----------------------------------------------------
*शिक्षण - बीएएमएस*
कालावधी - पाच वर्षे सहा महिने
पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, NEET
संधी कोठे? - स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालयात नोकरी
----------------------------------------------------
पुढील उच्च शिक्षण - एमडी, एमएस व इतर पदविका
----------------------------------------------------
*शिक्षण - बीएचएमएस*
कालावधी - पाच वर्षे सहा महिने
पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, NEET
संधी कोठे? - स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालयात नोकरी
----------------------------------------------------
पुढील उच्च शिक्षण - एमडी
----------------------------------------------------
*शिक्षण - बीयूएमएस*
कालावधी - पाच वर्षे सहा महिने
पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, NEET
संधी कोठे? - स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालयात नोकरी.
----------------------------------------------------
पुढील उच्च शिक्षण - पदव्युत्तर शिक्षण
----------------------------------------------------
*शिक्षण - बीडीएस*
कालावधी - चार वर्षे
पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, NEET
संधी कोठे? - स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालयात नोकरी
----------------------------------------------------
पुढील उच्च शिक्षण - एमडीएस
----------------------------------------------------
*शिक्षण - बीएससी इन नर्सिंग*
कालावधी - चार वर्षे
पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र NEET
संधी कोठे? - रुग्णालयात नर्स म्हणून नोकरी .
----------------------------------------------------
पुढील उच्च शिक्षण - पदव्युत्तर शिक्षण
----------------------------------------------------
*शिक्षण - बीव्हीएससी ऍण्ड एएच*
कालावधी - पाच वर्षे
पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र NEET
संधी कोठे? - प्राणी, जनावर रुग्णालयात नोकरी, प्राणी संग्रहालय, अभयारण्यात नोकरी, स्वतःचा व्यवसाय
पुढील उच्च शिक्षण - पदव्युत्तर शिक्षण
----------------------------------------------------
*शिक्षण - डिफार्म*
----------------------------------------------------
कालावधी - तीन वर्षे
पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, थेट प्रवेश
संधी कोठे? - औषधनिर्मिती कारखान्यात नोकरी, स्वतःचा व्यवसाय.
----------------------------------------------------
पुढील उच्च शिक्षण - बीफार्म
----------------------------------------------------
*शिक्षण - बीफार्म*
कालावधी - चार वर्षे
पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, सीईटी
संधी कोठे? - औषध कंपनी किंवा औषध संशोधन संस्था इत्यादी ठिकाणी नोकरी, स्वतःचा व्यवसाय, नागरी सेवा परीक्षा
पुढील उच्च शिक्षण - एमफार्म
------------------------------
संरक्षण दलांत प्रवेशासाठी
------------------------------
केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (यूपीएससी) वर्षातून एनडीए (एक) व एनडीए (दोन) अशा दोन वेळा लेखी परीक्षा होतात.
एअर फोर्स व नेव्हीसाठी जे उमेदवार राज्य शिक्षण मंडळाची किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बारावी परीक्षा भौतिकशास्त्र व गणित या विषयांसह उत्तीर्ण आहेत किंवा त्या परीक्षेस बसलेले आहेत, असे उमेदवार परीक्षेसाठी पात्र ठरतात.
वयोमर्यादा : साडेसोळा ते 19 वर्षांदरम्यान वय असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात.
------------------------------
*अभियांत्रिकी व ऑटोमोबाईल*
------------------------------
*शिक्षण - इंजिनिअरिंग डिप्लोमा*
कालावधी - तीन वर्षे
पात्रता व प्रवेश परीक्षा - बारावी शास्त्र, थेट दुसऱ्या वर्गात प्रवेश
संधी कोठे? - आयटी औद्योगिक क्षेत्रात, उद्योग किंवा व्यवसाय, स्वयंरोजगार
पुढील उच्च शिक्षण - बीईच्या दुसऱ्या वर्षात प्रवेश
*शिक्षण - बीई*
कालावधी - चार वर्षे
पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, सीईटी
संधी कोठे? - स्वतःचा व्यवसाय, आयटी, औद्योगिक क्षेत्र, संशोधन संस्था, नागरी सेवा परीक्षा, अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा
पुढील उच्च शिक्षण - एमई, एमटेक, एमबीए; तसेच जीआरई देऊन परदेशात एमएस
*शिक्षण - बीटेक*
कालावधी - चार वर्षे
पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, आयआयटी जेईई, एआयईईई
संधी कोठे? - औद्योगिक क्षेत्र, सरकारी उद्योग, खासगी उद्योग, संशोधन संस्था, आयटी क्षेत्र, नागरी सेवा व अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा, स्वयंरोजगार
पुढील उच्च शिक्षण - एमई, एमटेक, एमबीए किंवा जीआरई देऊन परदेशात एमएस
शिक्षण - ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकी पदवी -
कालावधी - चार वर्षे
पात्रता - बारावी शास्त्र, सीईटी
शिक्षण - ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकी पदव्युत्तर शिक्षण
कालावधी - दोन वर्षे
पात्रता - बीई, ऑटोमोबाईल, मॅकेनिकल, उत्पादन, तत्सम शिक्षण
बारावी नंतर काय विद्यार्थ्यांसाठी खास पोस्ट...................!*
----------------------------------------------------
*कॉम्प्युटरमधील कोर्सेस*
------------------------------
डीओईएसीसी "ओ' लेव्हल
कालावधी - एक वर्ष ऊजएअउउ
डिप्लोमा इन ऍडव्हान्स्ड सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी
कालावधी - दोन वर्षे
सर्टिफिकेट कोर्स इन इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी
कालावधी - सहा महिने
सर्टिफिकेट इन कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन
कालावधी - तीन महिने
सर्टिफिकेट इन कॉम्प्युटिंग
कालावधी - दहा महिने
इग्नू युनिव्हर्सिटी
सर्टिफिकेट कोर्स इन कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमिंग
कालावधी - एक वर्ष
----------------------------------------------------
*शिक्षण - बारावी*
------------------------------
*शास्त्र कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन*
कालावधी - एक वर्ष
वेब डिझाईनिंग ऍण्ड वेब डेव्हलपमेंट
कालावधी - दोन महिने
कॉम्प्युटर ऑपरेटर ऍण्ड प्रोग्रॅम असिस्टन्स
कालावधी - एक वर्ष
(फक्त मुलींसाठी)
डिप्लोमा इन ऍडव्हर्टायझिंग ऍण्ड ग्राफिक डिझाईनिंग
कालावधी - दोन वर्षे
गेम डिझाईन ऍण्ड डेव्हलपमेंट
कालावधी - एक वर्ष
प्रिंट इमेजिंग ऍण्ड पब्लिशिंग, कार्टून ऍनिमेशन, ई-कॉम डेव्हलपमेंट, वेब ग्राफिक्स ऍण्ड ऍनिमेशन
कालावधी - एक वर्ष
कॉम्प्युटर ऑपरेटर ऍण्ड प्रोग्रॅमिंग असिस्टंट
कालावधी - एक वर्ष
डेस्क टॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर
कालावधी - एक वर्ष
------------------------------
*रोजगाराभिमुख कोर्सेस*
------------------------------
*शिक्षण - डिप्लोमा इन प्लॅस्टिक मोल्ड टेक्नॉलॉजी*
कालावधी - तीन वर्षे
पात्रता - बारावी (70 टक्के)
संधी कोठे? - प्लॅस्टिक आणि मोल्ड
इंडस्ट्रीमध्ये संधी, सिंगापूर, मलेशियामध्ये संधी
उच्च शिक्षण - पदव्युत्तर शिक्षण
कोठे? सेंट्रल इन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लॅस्टिक्स
इंजिनिअरिंग ऍण्ड टेक्नॉलॉजी, म्हैसूर
*शिक्षण - टूल ऍण्ड डाय मेकिंग*
कालावधी - चार वर्षे
पात्रता - दहावी आणि बारावी पास
संधी - टूल ऍण्ड डाय इंडस्ट्री, भारत आणि मलेशियाशियामध्ये भरपूर संधी गव्हर्नमेंट टूल रूम ऍण्ड ट्रेनिंग सेंटर
(जीटीटीसी), नेट्टूर टेक्नॉलॉजी ट्रेनिंग
फाउंडेशन (एनटीटीएफ)
सेक्रेटरीअल प्रॅक्टिस
कालावधी - एक वर्ष
फॅशन टेक्नॉलॉजी
कालावधी - एक वर्ष
मॉडर्न ऑफिस प्रॅक्टिस
कालावधी - तीन वर्षे
------------------------------
*हॉस्पिटॅलिटी ऍण्ड टुरिझम*
------------------------------
*टूरिस्ट गाइड*
कालावधी - सहा महिने
डिप्लोमा इन फूड ऍण्ड बेव्हरेज सर्व्हिस
कालावधी - दीड वर्ष
बेसिक कोर्स ऑन ट्रॅव्हल फेअर ऍण्ड टिकेटिंग
कालावधी - तीन महिने
बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटराइज्ड रिझर्व्हेशन
सिस्टम (एअर टिकेटिंग)
कालावधी - एक महिना
अप्रेन्टाईसशिप
कालावधी - पाच महिने ते चार वर्षे
*शिक्षण - व्होकेशनल स्ट्रिममध्ये बारावी*
डिजिटल फोटोग्राफी
कालावधी - एक वर्ष
स्टोअर कीपिंग ऍण्ड पर्चेसिंग
कालावधी - एक ते तीन वर्षे
सेल्स ऍण्ड अकाउंटन्सी
कालावधी - एक ते तीन वर्षे.
------------------------------
*बांधकाम व्यवसाय*
------------------------------
*शिक्षण - बीआर्च*
कालावधी - पाच वर्षे
पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र,NATA , JEE
संधी कोठे? - स्वतःचा व्यवसाय किंवा बांधकाम उद्योगांमध्ये नोकरी, नागरी सेवा परीक्षा
पुढील उच्च शिक्षण - एमआर्च, एमटेक
*पारंपरिक कोर्सेस*
------------------------------
*शिक्षण - बीएससी*
कालावधी - तीन वर्षे
पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, प्रवेश थेट
संधी कोठे? - आयटी, औद्योगिक क्षेत्र, संशोधन संस्था, नागरी सेवा परीक्षा, स्वयंरोजगार
पुढील उच्च शिक्षण - एमएससी, एमबीए, एमसीए, एमपीएम इत्यादी.
------------------------------
*शिक्षण - बीएससी(Agri)*
कालावधी - 4 वर्षे
पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र व CET
संधी कोठे? - कृषी उद्योग कारखान्यात नोकरी, सरकारी कृषी सेवा नोकरी, नागरी सेवा परीक्षा, शेती व्यवसाय
पुढील उच्च शिक्षण - एमएससी (ऍग्रो), राष्ट्रीय कृषी परिषद संस्थांमध्ये संशोधन
*शिक्षण - बीए*
कालावधी - तीन वर्षे
संधी कोठे? - नोकरीसाठी व्यावसायिक, मृदू कौशल्ये, प्रमाणपत्र अथवा पदविका अभ्यासक्रम बीए करतेवेळी जास्त फायदेशीर. नागरी सेवा परीक्षा, स्वयंरोजगार
पुढील शिक्षण - एमए, एमबीए, पत्रकारिता, पदविका, एलएलबी
-----------------------------
*शिक्षण - बीकॉम*
कालावधी - तीन वर्षे
संधी कोठे? - आयसीडब्ल्यूए, सीए, सीएस परीक्षांचा अभ्यास बीकॉम करताना देणे फायदेशीर, नागरी सेवा परीक्षा, स्वयंरोजगार, लेखापाल म्हणून नोकरी
----------------------------------------------------
*शिक्षण - बीएसएल*
कालावधी - पाच वर्षे
संधी कोठे? - विधी व्यवसाय, विधी सल्लागार, नागरी सेवा परीक्षा, न्याय सेवा
पुढील उच्च शिक्षण - एलएलएम
------------------------------
*शिक्षण - डीएड*
कालावधी - दोन वर्षे
प्रवेश - सीईटी आवश्यक
संधी कोठे? - प्राथमिक शिक्षण शिक्षक
पुढील उच्च शिक्षण - बीए, बीकॉम व नंतर बीएड
----------------------------------------------------
*शिक्षण - बीबीए,* बीसीए,बीबीएम
कालावधी - तीन वर्षे
प्रवेश - सीईटी
संधी कोठे? - औद्योगिक क्षेत्रात नोकरी, आयटी क्षेत्रात नोकरी, स्वयंरोजगार, नागरी सेवा परीक्षा
पुढील उच्च शिक्षण - एमबीए, एमपीएम, एमसीए
------------------------------
*फॉरेन लॅंग्वेज*
(जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पॅनिश, चायनीज,
जॅपनीज, कोरियन)
कालावधी ः बेसिक, सर्टिफिकेट किंवा इतर
कोर्सेसवर आधारित
-----------------------------------------------------
*फॉर्म भरताना हे लक्षात ठेवा.......*
------------------------------
अर्ज भरायला जाताना मार्कलिस्ट, जातीचा दाखला, नागरिकत्व, आधार कार्ड आणि घराच्या पत्त्याच्या पुराव्याची अटेस्टेड कॉपी न्यायला विसरू नका.
पासपोर्ट आकाराचा फोटो, डिंक, त्याचबरोबर कागदपत्रे जोडण्यासाठी स्टेपलर जवळ ठेवा.
विद्यार्थ्यांचे नाव, पत्ता, ई-मेल, नागरिकत्व, जन्मतारीख, जन्मस्थळ इत्यादीची माहिती अर्जात दिलेल्या पद्धतीनेच भरावी. उदा.- आडनाव, पालकांचे नाव, स्वतःचे नाव योग्य रकान्यातच लिहावे. इंग्रजीमध्ये अर्ज भरल्यास तो कॅपिटल लेटरमध्ये भरावा.
अर्ज चुकू नये म्हणून सुरवातीला त्याच्या झेरॉक्सवर माहिती भरा. त्यानंतर अर्जात ती माहिती भरा. एखादा मुद्दा न कळल्यास मार्गदर्शन घ्या.
अर्ज भरायच्या तारखा आणि वेळापत्रकाचे कसोशीने पालन करा.
इतर क्षेत्रांमध्ये मिळवलेल्या प्रमाणपत्रांच्या अटेस्टेड कॉपी बरोबर ठेवा.
काही महाविद्यालयांमध्ये प्रश्नावली भरावी लागते. त्यामध्ये तुम्हाला याच महाविद्यालयामध्ये प्रवेश का हवा, ठराविकच शाखा का, रोल मॉडेल कोण, करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीजबाबत अनेक प्रश्न असतात. अशा प्रश्नांवरील उत्तरांचा आधीच विचार करून ठेवा.
बऱ्याच वेळेला ऑनलाइन अर्जप्रक्रिया पूर्ण करायच्या असतात. त्यासाठी संबंधित कागदपत्रे स्कॅन करा. ते पेनड्राइव्हवर सेव्ह करून ठेवा आणि तो आपल्या जवळ बाळगा.
-----------------------------
*काही महत्त्वाची संकेतस्थळे*
1) तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन.
(अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माण शास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट आदी)
www.dte.org.in
2) वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र शासन (वैद्यकीय शिक्षणासंबंधी)
www.dmer.org
3) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन (औद्योगिक प्रशिक्षणासाठी)
www.dvet.gov.in
4) पारंपरिक पदवी शिक्षण, पुणे विद्यापीठ
www.unipune.ac.in
5) भारतीय प्रौद्योगिक संस्था (आयआयटी), मुंबई
आयआयटी, जेईईसंबंधी (बी. टेक पदवी)
www.iitb.ac.in
6) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) "एआयईईई‘संबंधी अभियांत्रिकी शिक्षण
www.aipmt.nic.in
7) एनडीए प्रवेश परीक्षेणसंबंधी केंद्रीय लोकसेवा आयोगय (यूपीएससी)
www.upsc.gov.in वरील माहिती आपल्या मित्र,नातेवाईक,पाल्य,विद्यार्थी, यांना पाठवा.
🙏🏻👍
By
Dr.Ghapesh Pundalikrao Dhawale Nagpur
ghapesh84@gmail.com
8600044560
सोंजंन्य
AIDSO